“संवैधानिक व प्रशासनिक इतिहास”
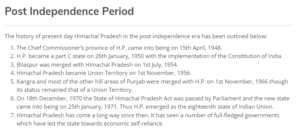
15 अप्रैल, 1948 को स्थापित होने के बाद हिमाचल प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे में जो बदलाव हुए, वे पहले ही बताए गए हैं. इस राज्य के चार जिलों का शासन मुख्यायुक्त को सौंपा गया था. श्री एन. सी. मेहता (ICS) पहले मुख्यमंत्री बने. श्री ई. पैडरल मून (I.C.S.) को उप-मुख्यायुक्त पद पर नियुक्त किया गया. 30 सितंबर, 1948 को एक सलाहकार समिति बनाई गई, जिसमें तीन पूर्व शासक और छह जनता के प्रतिनिधि थे, मुख्यायुक्त को सलाह देने के लिए; लेकिन समिति को कोई अधिकार नहीं था और उसकी सलाह को कोई बंधन नहीं था. मुख्य आयुक्त निर्णय स्वेच्छा से ले सकता था. जन नेताओं की उम्मीद थी कि संविधान सभा मुख्यायुक्त के अधीन राज्यों के लिए प्रजातांत्रिक प्रणाली बनाएगी, लेकिन इसे लोकसभा पर छोड़ दिया गया. लोकतांत्रिक प्रक्रिया की स्थापना के लिए सलाहकार समिति का समायोजन किया गया था, लेकिन मूलतः यह एक अयोग्य संस्था बन गया.
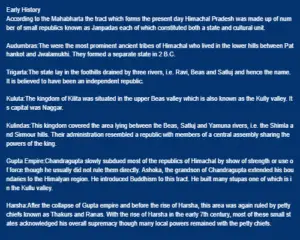
राज्य (भाग C) का “ग” भाग
26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया था. 1951 में हिमाचल प्रदेश को ‘ग’ भाग का राज्य बनाया गया था, लेकिन इसका शासन मुख्यायुक्त के अधीन ही रहा था. 1950 ई. को पैण्डरल मून प्रदेश का मुख्यायुक्त नियुक्त किया गया और पहले की तरह ही सलाहकार समिति की नियुक्ति की गई, लेकिन उनकी सलाह काम नहीं आई और उनके सदस्यों ने शीघ्र ही त्यागपत्र दे दिया. 1951 में श्री मून के स्थान पर श्री भगवान सहाय को मुख्यायुक्त बनाया गया, लेकिन पद्धति में दोष था.
डा. यशवंत सिंह परमार के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश के जन प्रतिनिधियों ने भारत सरकार को बताया कि ‘ग’ भाग में भी निर्वाचित सरकार होनी चाहिए. सितंबर 1951 में, भारतीय संसद ने ‘ग’ भाग के राज्यों में सीमित अधिकारों वाली निर्वाचित सरकारें बनाने का आदेश दिया।
पहला उप-राज्यपाल
(1.3.1952) पहला उप-राज्यपाल और पहली विधानसभा (24.3.1952): इस अधिनियम ने उप राज्यपाल और 36 सदस्यीय विधानसभा को मुख्यायुक्त की जगह दी. 1 मार्च 1952 को श्री हिम्मत सिंह को हिमाचल प्रदेश का पहला उप राज्यपाल बनाया गया था.
नवंबर 1951 में विधानसभा की 36 सीटों के लिए चुनाव हुए, जिसमें भारतीय कांग्रेस पार्टी ने 24 सीटें जीत कर बहुमत प्राप्त किया. डा. यशवंत सिंह परमार ने विधानसभा कांग्रेस दल का नेता चुना और 24 मार्च 1952 को हिमाचल प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री बन गया. महासु से स्वर्गीय श्री पद्म देव और मण्डी से श्री गौरी प्रसाद प्रदेश की पहली बार चुनी गई सरकार के दो अन्य मंत्री बने. 29 दिसंबर, 1953 को भारत सरकार ने राज्य पुनगर्ठन आयोग बनाने का फैसला किया और शीघ्र ही उसके सदस्यों को नियुक्त किया. न्यायमूर्ति फाजिल अली इसका अध्यक्ष और श्री के. एम. पाणिकर और श्री एच. एन. कुंजरू दो सदस्य नियुक्त किए गए.
राज्य पुनर्गठन आयोग ने 30 सितंबर 1955 को न्यायमूर्ति फाजिल अली को छोड़कर बहुमत से पंजाब में हिमाचल प्रदेश को शामिल करने की सिफारिश की. यदि ऐसा होता, तो सदियों से पिछड़े इस क्षेत्र का सारा विकास रुक जाता. डा. परमार के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश की जनता ने इस सिफारिश का विरोध किया. केंद्रीय नेता केवल एक बात पर इसे अलग रखने को राजी हुए: इसे केन्द्रीय शासित प्रदेश का दर्जा मिलेगा और कोई निर्वाचित सरकार नहीं होगी. हिमाचल प्रदेश के नेता इससे सहमत हो गए क्योंकि कोई चारा नहीं था. डा. परमार ने उस समय कहा कि हिमाचल प्रदेश का अस्तित्व बचाने के लिए कोई भी बड़ी कुर्बानी बड़ी नहीं होगी.
केन्द्रीय शासित प्रदेश (Union Territory)
1.11.56 से 24.1.71 तक: डा. परमार की सरकार ने 31 अक्टूबर, 1956 को त्यागपत्र दे दिया और हिमाचल प्रदेश 1 नवंबर, 1956 से एक केन्द्र शासित राज्य बन गया. स्वर्गीय बजरंग बहादुर सिंह (राजा भदरी, उत्तर प्रदेश) इस केन्द्र शासित प्रदेश के पहले उप-राज्यपाल बने. उन्होंने पहले 1.1.1954 से हिमाचल प्रदेश का उप-राज्यपाल किया था.
क्षेत्रीय परिषद्
December 1956 में भारतीय संसद ने क्षेत्रीय परिषद विधेयक पारित किया, जिसमें 41 सदस्यों की एक प्रदेशीय परिषद बनाई गई, जिसे जिला परिषद की तरह बनाया गया था. इसके सदस्यों को मई-जून, 1957 में चुना गया था. भारतीय कांग्रेस पार्टी ने इन चुनावों में बहुमत हासिल किया और 15 अगस्त, 1957 से परिषद् काम करने लगी. इस परिषद के 41 स्थानों में से 12 हरिजनों के लिए सुरक्षित थे. 2 सदस्य राष्ट्रपति चुन सकते थे. इसका कार्यकाल पांच वर्ष था. परिषद को हर दो महीने में कम से कम एक बार मिलना चाहिए था. इसके अलावा, किसी भी समय कुल सदस्यों का पांचवा भाग मांग कर बैठक बुला सकता था. अध्यक्ष को सदस्य बहुमत से चुन सकते थे या 2/3 बहुमत से निकाल सकते थे.
अध्यक्ष का पद संवैधानिक था. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष भी चुना गया था. इस परिषद् का अध्यक्ष मंडल के ठाकुर कर्म सिंह चुने गए। इस क्षेत्रीय परिषद् को बहुत कम अधिकार थे. यह उपराज्यपाल या परिषद् प्रशासक के अधीन था. उसके पास शिक्षा, स्वास्थ्य, पशुपालन और लोक निर्माण से जुड़े कुछ विभागों तक अधिकार थे। 300 रूपये मासिक वेतन वाले कर्मचारियों को ही नियुक्त करने का अधिकार था. सरकारी कर्मचारियों की तरह परिषद के कर्मचारी नहीं माने जाते थे. उप-राज्यपाल, प्रशासक के अधिकारों के साथ, शेष सभी अधिकार था. परिषद् को भंग करने का अधिकार भी प्रशासक को था.
विधानसभा की वापसी
इसके बाद, हिमाचल सहित केन्द्रीय शासित प्रदेशों के जन नेताओं ने निर्वाचित सरकारें बनाने के लिए संघर्ष जारी रखा. परिणामस्वरूप, 1962 में संविधान में चौदहवां संशोधन करने के बाद, भारतीय संसद ने 1963 में केन्द्र शासित प्रदेश अधिनियम पारित किया, जो केन्द्र शासित प्रदेशों में मौजूदा क्षेत्रीय परिषदों को विधानसभाओं में बदल देता था.
1 जुलाई, 1963 को हिमाचल प्रदेश क्षेत्रीय परिषद् को भी विधानसभा में बदल दिया गया. डा. यशवंत सिंह परमार ने फिर से विधानसभा बहुमत दल का नेतृत्व किया और 1 जुलाई 1963 को हिमाचल प्रदेश का दूसरा मुख्यमंत्री बन गया. सर्वश्री कर्मसिंह ठाकुर और हरिदास जी को उनकी सरकार में मंत्री बनाया गया. सितंबर 1965 में सरदार हुक्म सिंह की अध्यक्षता में भारत सरकार ने पंजाब को भाषा के आधार पर पुनर्गठित करने का सुझाव देने के लिए एक संसदीय कमेटी बनाई. इस समिति ने भाषा के आधार पर पंजाब को पुनर्गठित करने की सिफारिश की.
भारत सरकार ने मार्च 1966 में पंजाब को दो प्रातों (पंजाब और हरियाणा) में विभाजित करने की घोषणा की, साथ ही सीमा निर्धारित करने के लिए एक संस्था भी बनाई. डा. यशवंत सिंह परमार की हिमाचल सरकार ने इस आयोग के सामने पहाड़ी भाषी क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश में शामिल करने पर जोर दिया. इस आयोग का नेतृत्व न्यायधीश जे. सी. शाह ने किया था। परिणाम: हिमाचल प्रदेश 1 नवंबर 1966 को कांगड़ा, शिमला, नालागढ़ डलहौजी, कुल्लू, लहौल-स्पिति और होशियारपुर से ऊना आदि क्षेत्रों को अपने साथ मिलाकर बड़ा हो गया. विधानसभा में 41 की जगह 68 सदस्य हो गए. 1967 में चुनाव में भारतीय कांग्रेस पार्टी ने 37 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया. डॉ. यशवंत सिंह परमार को फिर से हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया.
पूरा राज्य मिल गया (25.1.1971)
हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था, जो इसके विकास को बहुत बाधित करता था. इस शासन में केंद्र का ही प्रभुत्व था और छोटी छोटी बातों के लिए केंद्र से मंजूरी लेनी पड़ती थी. अब अट हिमाचल नेतृत्व ने केन्द्रीय नेताओं पर जोर डालना शुरू कर दिया कि प्रांत को पूर्ण स्वायत्तता दी जाए. 24 जनवरी, 1968 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा ने एकमत से प्रस्ताव पारित करके राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की.
हिमाचल प्रदेश के सांसदों ने अगले साल 1969 में भारतीय संसद में एक गैर-सरकारी प्रस्ताव रखा जिसे बहुमत से समर्थन मिला. 31 जुलाई 1970 को, भारत की प्रधानमंत्री श्रीमति इन्दिरा गांधी ने हिमाचल को पूर्ण राज्य बनाने की संसद में घोषणा की, इस पर केंद्र सरकार ने अपनी नीति को पुनरावलोकन किया. भारतीय संसद ने 18 सितंबर 1970 को एक मत से इस संदर्भ में एक प्रस्ताव पारित किया. 25 जनवरी 1971 को, भारत की प्रधानमंत्री श्रीमति इन्दिरा गांधी ने शिमला में रिज के मैदान पर बर्फ की वर्षा के दौरान हिमाचल प्रदेश का भारतीय गणतंत्र का 18वां पूर्ण राज्य के रूप में उद्घाटन किया, जिसका नाम हिमाचल प्रदेश था. यही कारण था कि लोगों के लंबे और हिंसक आंदोलन का नेतृत्व श्रेष्ठ और शांत लोगों ने किया था. श्री एस. चक्रवर्ती हिमाचल प्रदेश के पहले पूर्ण राज्यपाल बने. 24 मार्च 1952 को डा. यशवंत सिंह परमार ने हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पद पर शपथ ली. प्रदेश स्तर पर सरकार के तीन प्रमुख अंग हैं: कार्यपालिका, विधान सभा और न्यायपालिका।